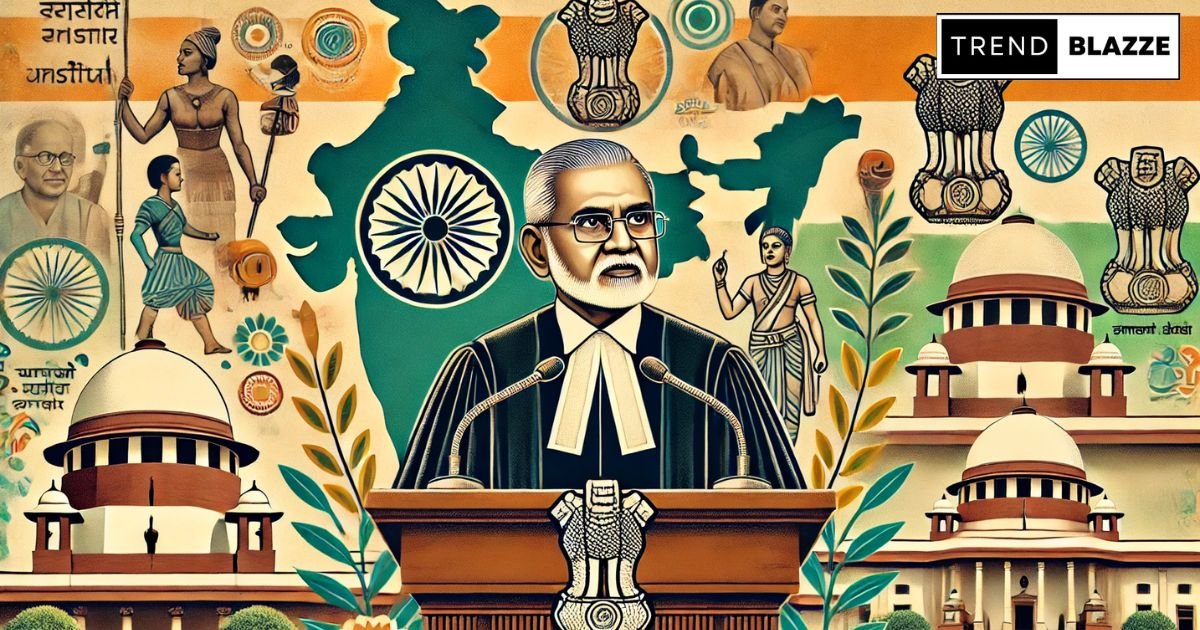भारत के मुख्य न्यायाधीश ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बयान दिया है कि देश में विविधता को बनाए रखने के लिए ‘संवैधानिक नैतिकता’ आवश्यक है। यह बयान संवैधानिक मूल्यों और नैतिकता की अहमियत को दर्शाता है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) में संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल होता है। यह केवल संविधान में लिखे गए शब्दों का ही पालन नहीं है, बल्कि इनके उद्देश्यों यानी इनकी वास्तविक भावना का भी पालन करना है। संवैधानिक नैतिकता संविधान की शाब्दिक व्याख्या से आगे जाकर संप्रभुता, सामाजिक न्याय एवं समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को भी शामिल करती है।
संवैधानिक नैतिकता का इतिहास:
संवैधानिक नैतिकता यानी कांस्टीट्यूशनल मोरैलिटी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे ने किया था। उन्होंने स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर जोर दिया था। इसके तहत नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने के साथ-साथ उनकी आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। संवैधानिक नैतिकता का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का सम्मान हो और सभी नागरिकों को समान अवसर मिले।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण:
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान के सुचारू रूप से काम करने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। हालांकि, यह कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया द्वारा विकसित होनी चाहिए। प्रशासन के स्वरूप और संविधान के स्वरूप के बीच एक मजबूत संबंध मौजूद होता है। जैसा कि संविधान के स्वरूप को बदले बिना, केवल प्रशासन के स्वरूप को बदलकर संविधान की भावना की उपेक्षा की जा सकती है। इस तरह संविधान को कमजोर किया जा सकता है। इसलिए, उन्होंने संविधान में ही प्रशासन के स्वरूप को तय करने का समर्थन किया था।
संवैधानिक नैतिकता से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान:
मूल अधिकार
मूल अधिकार राज्य द्वारा अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकार हैं। ये अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा प्रदान करते हैं और उन्हें मनमाने कार्रवाई से बचाते हैं। इन अधिकारों में स्वतंत्रता, समानता और धार्मिक स्वतंत्रता शामिल हैं, जो हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार हैं।
मूल कर्तव्य
मूल कर्तव्य देश के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति 11 कर्तव्य हैं। ये कर्तव्य नागरिकों को अपने देश और समाज के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं और उन्हें समाज में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। इनमें संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, और राष्ट्र की रक्षा करना आदि शामिल हैं।
शक्तियों का पृथक्करण
शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग-अलग करने का सिद्धांत है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करना आदि शामिल हैं। यह सिद्धांत संवैधानिक नैतिकता के पालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है।
संवैधानिक नैतिकता पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय:
कृष्णमूर्ति वाद (2015)
इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन आवश्यक है।
न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2018)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका की किसी भी कार्रवाई को निरस्त करके संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने के अपने कर्तव्य को दोहराया था। इस निर्णय ने संवैधानिक नैतिकता की महत्ता को और भी स्पष्ट किया।
नवतेज सिंह जौहर वाद (2018)
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को गैर-आपराधिक बनाकर सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी थी। इस निर्णय ने यह साबित किया कि संविधान के सिद्धांत और मूल्य सामाजिक धारणाओं से ऊपर हैं।
निष्कर्ष:
संवैधानिक नैतिकता भारत के संवैधानिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह केवल संविधान के शब्दों का पालन नहीं है, बल्कि इसके उद्देश्यों और मूल्यों की रक्षा और पालन करना भी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह बयान देश में संवैधानिक नैतिकता की आवश्यकता और महत्ता को रेखांकित करता है। विविधता, समानता और न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन आवश्यक है। इस प्रकार, संवैधानिक नैतिकता न केवल संवैधानिक संस्थाओं की निष्ठा को बनाए रखती है, बल्कि यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की भी याद दिलाती है।
FAQs:
संवैधानिक नैतिकता क्या है?
संवैधानिक नैतिकता (Constitutional Morality) में संवैधानिक मानदंडों का पालन करना शामिल होता है। यह केवल संविधान में लिखे गए शब्दों का ही पालन नहीं है, बल्कि इनके उद्देश्यों यानी इनकी वास्तविक भावना का भी पालन करना है। संवैधानिक नैतिकता संविधान की शाब्दिक व्याख्या से आगे जाकर संप्रभुता, सामाजिक न्याय एवं समानता जैसे संवैधानिक मूल्यों की प्रतिबद्धता को भी शामिल करती है।
संवैधानिक नैतिकता का इतिहास क्या है?
संवैधानिक नैतिकता शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग ब्रिटिश इतिहासकार जॉर्ज ग्रोटे ने किया था। उन्होंने स्वतंत्रता और प्रतिबंधों के बीच संतुलन पर जोर दिया था। इसके तहत नागरिकों को संवैधानिक संस्थाओं के प्रति निष्ठा प्रकट करने के साथ-साथ उनकी आलोचना करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता क्यों महत्वपूर्ण है?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले संविधान के सुचारू रूप से काम करने के लिए संवैधानिक नैतिकता आवश्यक है। यह कोई स्वाभाविक या प्राकृतिक भावना नहीं है, बल्कि यह एक सतत प्रक्रिया द्वारा विकसित होनी चाहिए। उन्होंने संविधान में ही प्रशासन के स्वरूप को तय करने का समर्थन किया था ताकि संविधान की भावना की उपेक्षा न हो सके।
मूल अधिकार और मूल कर्तव्य क्या हैं?
मूल अधिकार राज्य द्वारा अपनी शक्ति के मनमाने उपयोग के खिलाफ नागरिकों के अधिकार हैं। ये अधिकार नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल कर्तव्य देश के नागरिकों के राष्ट्र के प्रति 11 कर्तव्य हैं, जो उन्हें अपने देश और समाज के प्रति उनके दायित्वों की याद दिलाते हैं।
शक्तियों का पृथक्करण क्या है?
शक्तियों का पृथक्करण विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को अलग-अलग करने का सिद्धांत है। इसमें विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों की निगरानी करना आदि शामिल हैं। यह सिद्धांत संवैधानिक नैतिकता के पालन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सुप्रीम कोर्ट के कौन से निर्णय संवैधानिक नैतिकता को महत्वपूर्ण मानते हैं?
1. कृष्णमूर्ति वाद (2015): इस मामले में शीर्ष न्यायालय ने सुशासन के लिए संवैधानिक नैतिकता का पालन आवश्यक बताया।
2. न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टास्वामी वाद (2018): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को निरस्त करके संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने का अपना कर्तव्य दोहराया।
3. नवतेज सिंह जौहर वाद (2018): इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने IPC की धारा 377 के तहत समलैंगिक संबंधों को गैर-आपराधिक बनाकर सामाजिक नैतिकता की तुलना में संवैधानिक नैतिकता को वरीयता दी।